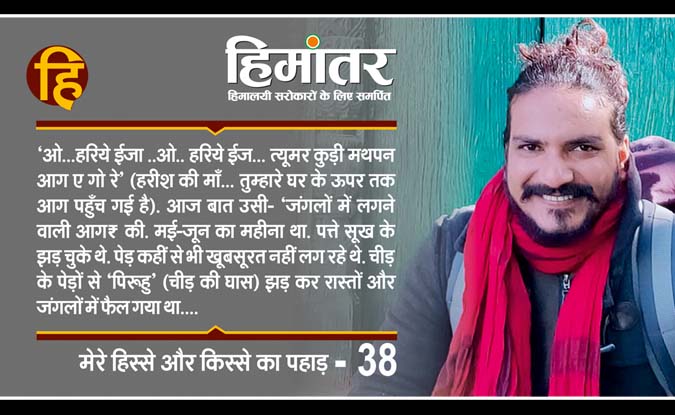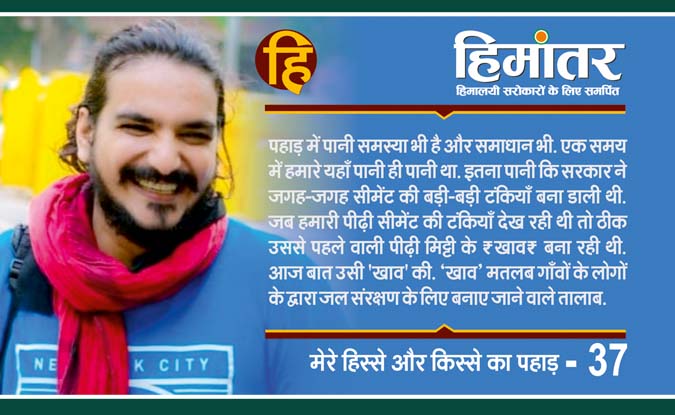विश्व-साहित्य के युगनायक- प्रेमचन्द, गोर्की और लू शुन
मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिन पर विशेषडॉ. अरुण कुकसालप्रेमचंद, गोर्की और लू शुन तीन महान साहित्यकार, कलाकार और चिंतक. जीवनभर अभावों में रहते हुए अध्ययन, मनन, चिन्तन और लेखन के जरिए बीसवीं सदी के विश्व-साहित्य के युगनायक बने. एक जैसे जीवन संघर्षों के कारण तीनों वैचारिक साम्यता, स्वभाव और व्यवहार के भी करीब थे. पढ़ने-लिखने का चस्का तीनों पर बचपन से था. प्रेमचन्द के पहले अध्यापक एक मौलवी थे जो उन्हें उर्दू-फारसी सिखाते थे. गोर्की ने अपनी नानी से सुनी कहानियों की हकीकत जानने की जिज्ञासा से पढ़ना शुरू किया. लू शुन मेघावी छा़त्र थे इस कारण पढ़ने का जनून उनमें बचपन से ही था. तीनों के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था. निर्धनता के कारण पढ़ने के लिए कई कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा था. पर अपनी स्वाध्याय के प्रति जबरदस्त जिद्द के कारण उन्होनें हर मुसीबत का डटकर मुकाबला किया था.जनवादी लेखक हंसर...