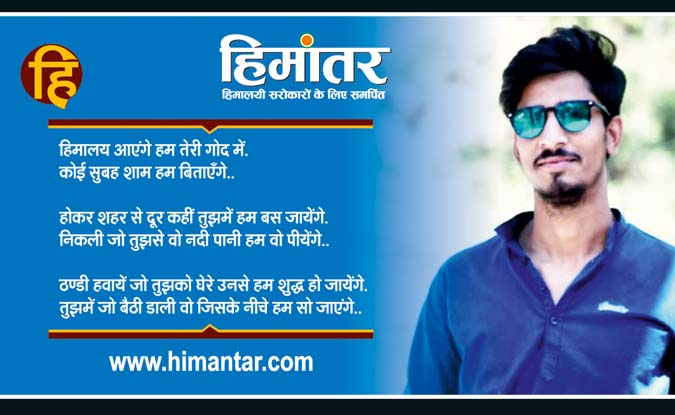Month: August 2020

‘हे दरी हिमाला दरी ताछुम’
डॉ. अमिता प्रकाश“हे दरी हिमाला दरी ताछुम-ताछुमा-छुम.
दरी का ऐंगी सौदेर दरी ताछुम-ताछुमा-छुम”..
हाथों से एक दूसरे की बाँह पकड़कर घेरे में गोल-गोल घूमकर दो कदम आगे बढ़ाते हुए धम्म से कूदती हुई लड़कियों को देखकर छज्जे में बैठी मेरी नानी, मामी और दूसरी लड़कियों की दादी, बोडी (ताई), काकी (चाची) की टिप्पणियाँ हमें उस समय बहुत चिढ़ाती थीं, क्योंकि अक्सर वह अपने खेलों की तुलना हमारे खेलों से करती हुई हमें कमतर ही घोषित करतीं, हर पुरानी पीढ़ी की तरह यह कहते हुए कि “हमर जमाना म त इन्न नि होंदु छौ, या इन होंदु छौ” (हमारे जमाने में तो ऐसा होता था या ऐसा नही होता था.) और हम नयी पंख निकली चिड़ियाओं जैसे उत्साह में उनका मुँह चिढ़ातीं अक्सर कह उठतीं “अपड़ जमने र्छुइं तुम अफिम रैण द्यावा... हमल त इन्नी ख्यलण” (अपने जमाने की बातें तुम अपने ही पास ही रहने दो, हम तो ऐसी ही खेलेंगे). पीढ़ी के अंतर से उपजी यह मतभिन...

खनार
कहानीडॉ. कुसुम जोशीरमा कान्त उर्फ रमदा के बिल्कुल सड़क से सटे घर के आंगन में कार को पार्क कर उनकी छोटी सी परचून की दुकान में उनसे मुलाकात करने के लिये आगे बढ़ गया. बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे हम. दो साल सीनियर थे मुझसे, पढ़ने में अच्छे थे पर पुरोहिताई करने वाले पिता असमय ही चल बसे. किसी तरह दो साल मां की मेहनत, थोड़ा-सा मलकोट का सहारा था जो इंटर कर ही लिया, इंटर के बाद अल्मोड़ा चले गये. किसी दुकान में काम करने लगे.
उन पर ईश्वर कृपा इतनी ही रही कि 'दिल्ली मुम्बई' जाने की प्रेरणा नही मिली.घर के सयाने थे हर समय मां छोटे भाई बहनों की चिन्ता सताती थी.पगार भी इतनी भर की अपना ही खर्च खींच तान के निकल पाता.पर एक बड़ी उपलब्धि ये हुयी कि दुकान में काम करते दुकानदारी सीख ली. दो साल बाद आत्मविश्वास आते ही गांव लौट आये और गांव में किराने की छोटी सी दुकान शुरु की .सफर ठीक-ठाक ही रहा. ...
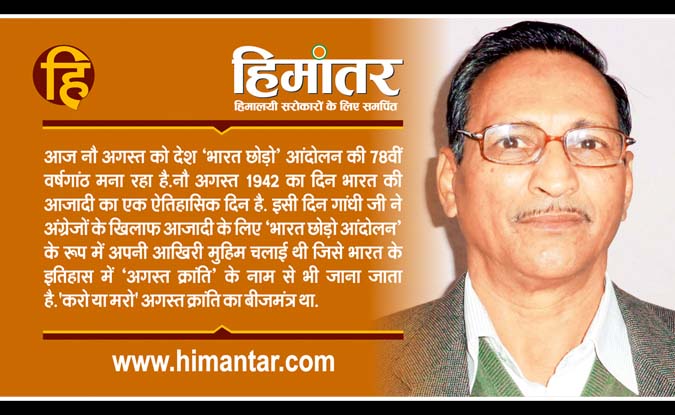
‘करो या मरो’ अगस्त क्रांति का बीजमंत्र
9 अगस्त 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर विशेषडॉ. मोहन चंद तिवारीआज नौ अगस्त को देश 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है.नौ अगस्त 1942 का दिन भारत की आजादी का एक ऐतिहासिक दिन है. इसी दिन गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए “भारत छोड़ो आंदोलन” के रूप में अपनी आखिरी मुहिम चलाई थी जिसे भारत के इतिहास में 'अगस्त क्रांति' के नाम से भी जाना जाता है.'करो या मरो' अगस्त क्रांति का बीजमंत्र था. महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चले इस विशाल जन आन्दोलन के जरिए अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति चाहने वाले करोड़ों देशभक्तों ने अपना तन मन धन न्योछावर करते हुए ब्रिटिश शासन की चूल को हिलाकर रख दिया था. बाद में इसी आंदोलन ने 1947 में मिली आजादी की नींव भी रखी.1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड के 21 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए और हजारों को गिरफ्तार किया गया,जिसके परिण...

रिंगाल: उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हरा सोना
जे. पी. मैठाणीपहाड़ की अर्थव्यवस्था के साथ रिंगाल का अटूट रिश्ता रहा है. रिंगाल बांस की तरह की ही एक झाड़ी है. इसमें छड़ी की तरह लम्बे तने पर लम्बी एवं पतली पत्तियां गुच्छी के रूप में निकलती है. यह झाड़ी पहाड़ की संस्कृति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण वनस्पति समझी जाती है. पहाड़ के जनजीवन का पर्याय रिंगाल, पहाड़ की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ अंग रहा है. प्राचीन काल से ही यहाँ के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का श्री गणेश रिंगाल की बनी कलम से होता था. घास लाने की कण्डी से लेकर सूप, टोकरियां, चटाईयां, कण्डे, बच्चों की कलम, गौशाला, झोपडी तथा मकान तक में रिंगाल अनिवार्य रूप में लगाया जाता है.
वानस्पतिक परिचय-
वन विभाग के अनुसार रिंगाल एक वृक्ष है, परन्तु वन विभाग की 1926-1928 से सन् 1936-37 की कार्य योजना में रिगाल की परिभाषा-
“रिंगाल एक बहुवर्षीय पेड़ों के नीचे उगने वाली झाड़ी/ घास है जो नोड्स एवं इन्टर नोड्स म...
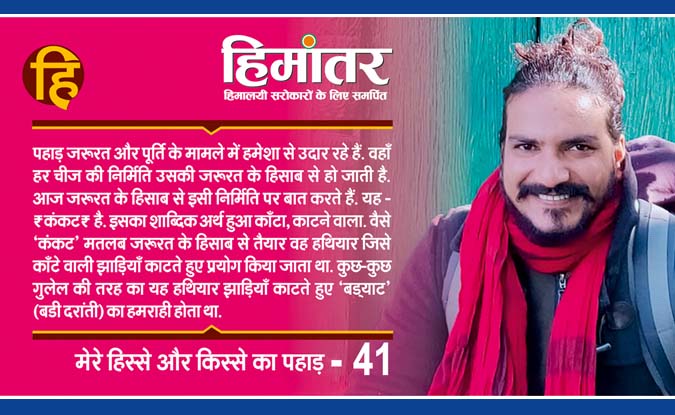
कंकट सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि पहाड़ की विरासत का औज़ार है
मेरे हिस्से और पहाड़ के किस्से भाग—41प्रकाश उप्रेतीपहाड़ जरूरत और पूर्ति के मामले में हमेशा से उदार रहे हैं. वहाँ हर चीज की निर्मिति उसकी जरूरत के हिसाब से हो जाती है. आज जरूरत के हिसाब से इसी निर्मिति पर बात करते हैं. because यह -"कंकट" है. इसका शाब्दिक अर्थ हुआ काँटा, काटने वाला. वैसे 'कंकट' मतलब जरूरत के हिसाब से तैयार वह हथियार जिसे काँटे वाली झाड़ियाँ काटते हुए प्रयोग किया जाता था. कुछ-कुछ गुलेल की तरह का यह हथियार झाड़ियाँ काटते हुए "बड्याट" (बडी दरांती) का हमराही होता था. दोनों की संगत ही आपको काँटों से बचा सकती थी. इनकी संगत के बड़े किस्से हैं.
ज्योतिष
कंकट बहुत लंबा नहीं होता था. एक हाथ भर का ही बनाया जाता था. ईजा कुछ छोटे और कुछ बड़े बनाकर रखे रहती थीं. because रखने की जगह या तो 'छन' की छत होती थी या फिर जहाँ सभी छोटी-बड़ी दराँती रखी रहती थीं, वहाँ होती थी. अमूमन तो सूखी लक...

इजा! नि थामि तेरी कईकई, सब जगां रई तेरी नराई
(शम्भूदत्त सती का व्यक्तित्व व कृतित्व-3)डॉ. मोहन चंद तिवारीकुमाऊं के यशस्वी साहित्यकार शम्भूदत्त सती की रचनाधर्मिता से पहाड़ के स्थानीय लोग प्रायः कम ही परिचित हैं किन्तु पिछले तीन दशकों से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक आंचलिक कुमाऊंनी साहित्यकार के रूप में सती जी ने अपनी एक खास पहचान बनाई है. शम्भूदत्त सती साहित्य की सभी विधाओं में लिखते रहे हैं. कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक और यहां तक की रेखाचित्र विधाओं में भी. पिछले 27 वर्षों से विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं.इनकी सभी कृतियों में पहाड़ के भोगे हुए संघर्षपूर्ण जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है. वहां की लोक संस्कृति, पर्व-उत्सव, लोकगीत, ग्रामीण जीवन, विवाह गीत, झाड़- फूंक के मंत्र, और कुमाऊंनी शब्द सम्पदा आदि का वर्णन अत्यंत रोचक और मनोहारी शैली में किया गया है.पहाड़ की लोकसंस्कृति के संस्कार...