‘बाटुइ’ लगाता है पहाड़, भाग—13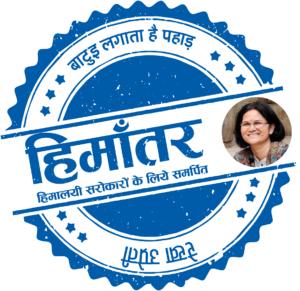
- रेखा उप्रेती
“जोर का मंडान लग गया रे! जल्दी-जल्दी हिटो” संगिनियों के साथ धुर-धार से लौटती टोली के कदम तेज हो उठते. ‘मंडान’ मतलब चारों तरफ़ से बादलों का घिर आना. बौछारों की अगवानी से पूर्व आकाश में काले मेघों का चंदोवा…
घसियारिनें अपनी दातुली कमर में खोस लेतीं, लकडियाँ बीनती काखियाँ गट्ठर बाँधने लगतीं, खेतों में निराई-गुड़ाई करती जेड्जा कुटव चलाना छोड़ देती… पर कितनी ही दौड़ लगा लें, घर पहुँचने तक इन सबका भीग कर फुत-फुत हो जाना तय होता.
मंडान देखकर घर में भी हका-हाक शुरू… आँगन में सूखते धान, बड़ियाँ, मिर्चें उठानी हैं, टाल में से सूखी लकडियाँ उठाकर गोठ रखनी हैं, पुआल के लुटों से गट्ठर उठाकर छान में रखना है. मल भितेर के पाख में रोशनी देने के लिए बना जा’व बंद करने के लिए उसका पाथर खिसकाना है. आँगन में जहाँ-जहाँ पाख से बारिश की बंधार लगेगी, उसके नीचे बर्तन धरने हैं ताकि पानी इकठ्ठा हो सके, अन्दर जहाँ-जहाँ छत टपकती है वहाँ लोटा या तौली लगाना … ये सब करने का मौका देता मंडान और फिर बरसने लगता…
मंडान में बहुत सुन्दर लगता पहाड़ … एक साँवला रंग पूरे परिवेश को अपनी आगोश में ले लेता. पेड़-पौधे स्तब्ध, हवा ठहरी सी, पंछी कहीं दुबके हुए, मनुष्य अपनी हलचल समेट सिमटा हुआ … सब प्रतीक्षा में …आकाश के रंगमंच की तीसरी घंटी बजे और वर्षा का नर्तन शुरू हो…
वे घास काट कर छोड़ आये थे और लेने जा रहे थे… मेरा भी मन मचल उठा. दीदी ने मना किया, मैं मानी नहीं तो एक चपत लगा दी मेरे गाल पर… मैं स्तब्ध रह गयी… इसके अलावा कभी कोई चपत खायी हो, याद नहीं पड़ता.
ऐसे ही किसी एक मंडान में मैंने जिद पकड़ ली कि पौर की चाची और अपनी हमउम्र चचेरी बहन के साथ मुझे भी गधेरे तक जाना है. वे घास काट कर छोड़ आये थे और लेने जा रहे थे… मेरा भी मन मचल उठा. दीदी ने मना किया, मैं मानी नहीं तो एक चपत लगा दी मेरे गाल पर… मैं स्तब्ध रह गयी… इसके अलावा कभी कोई चपत खायी हो, याद नहीं पड़ता.

ये मझली दीदी मेरे उस बचपन का अटूट हिस्सा थी. पिता जी दिल्ली में, बड़ी दीदी ससुराल, छोटी दीदी और भाई भी पढ़ाई के वास्ते दूर … माँ से भी माँ जैसा लगाव नहीं था उन दिनों… तो मेरी ‘पितु मातु सहायक स्वामी सखा’ यही दीदी थी. उस दिन चपत खाकर मैं रोती या नहीं, दीदी खुद ही रोने लगी…फिर घर में जो भी दाड़िम-चिवड़े-आखोड़-मिश्री जैसी नेमतें उपलब्ध थीं, ला-लाकर मेरी अँजुरी में भरती रही.
उस दिन के बाद मैंने कभी कोई जिद नहीं पकड़ी…
ऐसे ही मोहक मंडान का नज़ारा लेते हुए एक और काण्ड किया मैंने… पहाड़ी मकानों के ऊपरी तल में झज्जे होते हैं… नक्काशीदार लकड़ी से बने… झज्जे का निचला एक चौथाई हिस्सा बंद होता है और उसके चार अंगुल ऊपर एक मोटी छड़ लगी होती है जिसे पकड़कर नीचे झाँका जाता है… तो उस डंडे पर बैठना, मेरा साधा हुआ अभ्यास था. दोनों पैरों के तलवे उस पर टिका, उकडू बैठकर, हाथों से घुटनों को समेटे एकदम साधक के से संतुलन से टिकी रहती उस पर… जब बारिश का मंडान लगता तो वहाँ से बेहद खूबसूरत दृश्य दीखता सामने… अब तो सोचकर भी डर लगता है कि कहीं गिर जाती तो…
… तो गरम पानी से सिकाई हुई, गर्म-गर्म हलवा बना कर खिलाया गया. मन ‘झसक’ गया होगा, सोचकर शाम को पौर के बड़बाज्यू ने ‘बिभूत’ लगा दिया… हो गया तन और मन दोनों का इलाज़ … आज तक लड़की भली-चंगी खड़ी है.
तो क्या! गिर ही तो गयी उस दिन… माँ और दीदी मंडान देख आँगन से कुछ समेटने में लगे थे और मैं आँखों से समेट रही थी पहाड़ों पर घिर आए घने बादलों के साये … एकदम ध्यानमग्न-सी… तभी पीछे से एक नन्हे बच्चे ने मुझे छू कर पुकारा ‘मौसी’
और मौसी धड़ाम से नीचे…

धम्म की हल्की आवाज़ से माँ को लगा कोई घास का गट्ठर गिरा है, देखा तो लड़की गठरी बन बैठी थी. सर के बल गिरती तो वहीं चित्त पायी जाती पर जाने किस की कृपा से ऐसे गिरी जैसे गोद में लेकर बीच आँगन में बिठा दिया हो किसी ने. उठा भीतर ले गए … कहाँ का एक्स-रे, कैसा डॉक्टर, किसका अस्पताल, कौन-सी दवाई …इन सब का तो ख़याल भी नहीं आया किसी को, आता भी तो वहाँ कौन-सा ये सुविधाएँ उपलब्ध थीं … तो गरम पानी से सिकाई हुई, गर्म-गर्म हलवा बना कर खिलाया गया. मन ‘झसक’ गया होगा, सोचकर शाम को पौर के बड़बाज्यू ने ‘बिभूत’ लगा दिया… हो गया तन और मन दोनों का इलाज़ … आज तक लड़की भली-चंगी खड़ी है.
बादलों से खूब आँख-मिचौली भी खेली … छज्जे से दीखता कि नीचे आँगन से लेकर पूरी घाटी तक बादल की हलकी-हलकी परतें बिछी हैं… सीढ़ियाँ उतर नीचे आँगन में जाकर देखते तो वहाँ कुछ भी नहीं … बादल तो पौर की आमा के आँगन में खेल रहा है या नीचे के बाड़े में कूद गया है. आमा के आँगन में पहुँचो तो वहाँ से भी गायब… अपने ही चारों तरफ़ नज़र घुमाओ तो सब तरफ़ वही-वह, बस हाथ में आना मंज़ूर नहीं… ऊपर खरा निथरा आकाश, पेड़ों की धुली-धुली फुगनियाँ, बादलों की सफ़ेद चादर ओढ़े पहाड़ियों के शिखर भर झाँकते दिखते… कभी-कभी ढलान पर लेटे-लेटे ऊपर आकाश के परदे पर बादलों के चल-चित्र देख कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाते… कितनी सारी बनती-बिगड़ती आकृतियाँ ….
बरसते बादल हमेशा भले नहीं लगते थे, खासकर जब कई दिनों तक लगातार ‘झड़’ पड़ जाते… हमें ठिठुरते हुए अन्दर बंद रहना पड़ता. छत की बल्लियों पर पानी की बूँदें जमा होतीं, खिसकतीं और टपकती रहतीं, नीचे रखे पीतल के तोले में टप्प-टप्प और कभी टन आवाज़ आती… हम सब चाख में बैठ छज्जों से देखते, बाहर बौछारों की तांडव-लीला…

आषाढ़ लगता तो इस प्रिय पाहुने की इंतज़ार में रहते सब … “ मानसिंग कब आ रहा है रे!” मलकुड़ की आमा काका से पूछती… रेडियो पर मानसून के आने की आहट ख़बर बनकर फैलती थी. सबकी कमर कस जाती. बारी-बारी सबके खेतों में रोपाई का ‘पल्ट’ लगता. पानी से भरे खेत दर्पण-सी चमक मारते… उन पर झुकी पलटन एक लय में पीछे-पीछे खिसकती हुई धान रोपती… एक मुट्ठी में बिनौड़ (पौध) का गट्ठर दूसरे हाथ से एक-एक पौधे को रोपते, दलदल-सी मिट्टी में धँसे पैर छुड़ा, उन्हें पीछे ले जाने की क्रिया कुशल बाजीगरी सरीखी होती. हम भी बीच में घुसकर अपनी हौंस पूरी करते… पर थोड़ी देर बाद पता लगता कि अटक गए हैं, पलटन गीत गाती पीछे सरक गयी और हमें ‘गोठ’’ में डाल दिया…
बरसते बादल हमेशा भले नहीं लगते थे, खासकर जब कई दिनों तक लगातार ‘झड़’ पड़ जाते… हमें ठिठुरते हुए अन्दर बंद रहना पड़ता. छत की बल्लियों पर पानी की बूँदें जमा होतीं, खिसकतीं और टपकती रहतीं, नीचे रखे पीतल के तोले में टप्प-टप्प और कभी टन आवाज़ आती… हम सब चाख में बैठ छज्जों से देखते, बाहर बौछारों की तांडव-लीला… बड़े-बड़े पेड़ भी नतशिर हो उठते… सामने की पहाड़ियों से पानी के कई ‘रौल’ यानी झरने से छूटते रहते, कई बार ढलान पर उगे पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ डालते ये रौल… बिजली कड़कती, बज्र गिरने की संभावना से डरे रहते … भीतर जलती ‘सगड़’ को घेर आग तापते, सुनी-सुनाई पहेलियाँ, कहानियाँ दोहराते… तब न बाज़ार जाना संभव होता न अपने बाड़े में उगी सब्जियाँ तोड़ लाना… इन्हीं दिनों के लिए काटकर सुखाई गयीं हरी सब्जियां, कस कर सुखाई मूली, कद्दू के ख्वेड, ककड़ी और पापड़ की बड़ियाँ, भट, गहत, रैंस, मडुआ, झुंगर भोजन की भूमिका निभाता… माँ बताती थी कि उनके बचपन में जब ‘सत-झड़’ पड़ते तो भट या सोयाबीन को भूनकर भीतर फैला दिया जाता. छोटे बच्चे उन्हें ढूँढ-ढूँढ कर खाते रहते … उनका समय भी कटता और भूख भी…
वही है जो मैदानों में बह आए पानी को अपनी कसेरी-गगरी में भर-भरकर वापस ले आता है, बरसता, भिगाता, नौलों-धारों-गधेरों-गाड़ों को जीवन देता, सूखते स्रोतों को जिलाता… बादल समझता है अपनी जिम्मेदारी… हम मैदानों में उतर आए लोग कब समझेंगे…!!
बादल आपदा बनकर भी बरसता पहाड़ पर… रौल की चपेट में आकर खेत बह जाते, कभी धँस जाते, खिसक जाते… ‘गाड़’ आती तो लकड़ी का एकमात्र पुल हर साल टूट कर बह निकलता, गाड़ के किनारे-किनारे वाले खेतों में अनुपजाऊ गाद भर जाता … कई जन और जानवर भी चपेट में आ जाते कभी… कुछ वर्ष पहले केदारनाथ में आई भयावह आपदा के घाव तो अब भी नहीं भरे हैं… कभी बागेश्वर, कभी धौलाड़, कभी पिथौरागड़ में बादल फटने की खबर दहला देती है….
पर फिर भी बादल वरदान है पहाड़ के लिए… वही है जो मैदानों में बह आए पानी को अपनी कसेरी-गगरी में भर-भरकर वापस ले आता है, बरसता, भिगाता, नौलों-धारों-गधेरों-गाड़ों को जीवन देता, सूखते स्रोतों को जिलाता…
बादल समझता है अपनी जिम्मेदारी… हम मैदानों में उतर आए लोग कब समझेंगे…!!
(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के इन्द्रप्रस्थ कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं)

