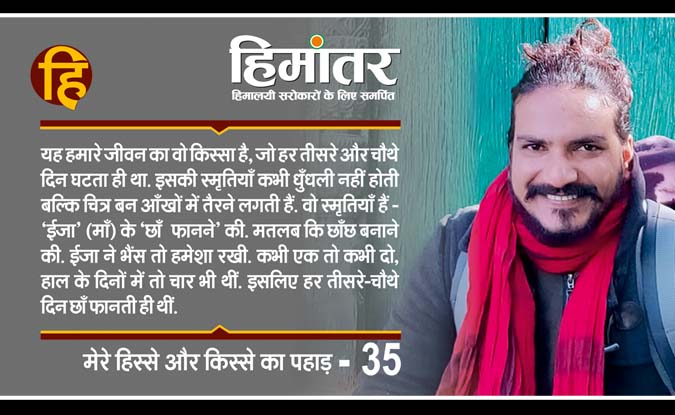मेरे हिस्से और पहाड़ के किस्से भाग—35
- प्रकाश उप्रेती
यह हमारे जीवन का वो किस्सा है, जो हर तीसरे और चौथे दिन घटता ही था. इसकी स्मृतियाँ कभी धुँधली नहीं होती बल्कि चित्र बन आँखों में तैरने लगती हैं. वो स्मृतियाँ हैं -‘ईजा’ (माँ) के ‘छाँ फ़ानने’ की. मतलब कि छाँछ बनाने की. ईजा ने भैंस तो हमेशा रखी. कभी एक तो कभी दो, हाल के दिनों में तो चार भी थीं. इसलिए हर तीसरे-चौथे दिन छाँ फानती ही थीं.
ईजा ‘भतेर’ (घर का ऊपर वाला हिस्सा) ‘थुमी’ (घर के बीच में धुरी के समान लगी मोटी लकड़ी) पर छाँ फानती थी. थुमी पर दो ‘ज्योड़’ (रस्सी) जिन्हें “नेतण” कहा जाता था, हमेशा बंधे रहते थे. ईजा उनमें ‘रअडी’ ( एक लंबी लकड़ी जिसके नीचे के सिरे पर तिकोना बनाया होता था) को फंसाकर ‘कंटर’ (कनस्तर) में छाँ फानती थीं. उसको बीचों-बीच में करना और बैलेंस बनाए रखना भी कला होती थी. तब घर की नई बहू की परीक्षा ‘छाँ’ फानना आता है कि नहीं इस बात से भी ली जाती थी.
 ईजा जब भी छाँ फानती थीं तो हम वहीं पर बैठे रहते थे. बस ईजा को छाँ फानते हुए एकटक देखते रहते थे. फानते हुए घूर… घवां… की आवाज आती थी. ईजा हमेशा कहती थीं- “गोधनी ईजा छाँ कसि फाने” ( गोधनी की माँ छाँछ कैसे बनाती थी?) हम कहते थे- “घूर… घवां…”. यह छाँ फानते हुए का रोज का किस्सा होता था. कभी-कभी हम भी उसमें हाथ अजमाते थे लेकिन वो बैलैंस नहीं बन पाता था. न ही वो लय पकड़ पाते थे, जिस लय में ईजा फानती रहती थीं. न धीमे न तेज, बस घूर… घवां…
ईजा जब भी छाँ फानती थीं तो हम वहीं पर बैठे रहते थे. बस ईजा को छाँ फानते हुए एकटक देखते रहते थे. फानते हुए घूर… घवां… की आवाज आती थी. ईजा हमेशा कहती थीं- “गोधनी ईजा छाँ कसि फाने” ( गोधनी की माँ छाँछ कैसे बनाती थी?) हम कहते थे- “घूर… घवां…”. यह छाँ फानते हुए का रोज का किस्सा होता था. कभी-कभी हम भी उसमें हाथ अजमाते थे लेकिन वो बैलैंस नहीं बन पाता था. न ही वो लय पकड़ पाते थे, जिस लय में ईजा फानती रहती थीं. न धीमे न तेज, बस घूर… घवां…
ईजा हमको ताजी छाँ देती थीं तो हम दो-तीन गिलास पी जाते थे. छाँ खत्म होने पर खाली गिलास में जोर का ‘सुड़ूक’ (खाली गिलास से आवाज निकालते) मारते थे. ईजा बीच में पूछ लेती थीं- “खटि नि है रे”, नतर लूण धर ले’ (खट्टी तो नहीं हो रही है, नहीं तो नमक रख ले).
ईजा छाँ फानते हुए हमें कहती थीं-“इथां झन देखिए हां, हाक लागि ज्यालि”(इधर मत देखना, नज़र लग जाएगी). तभी ईजा हमको कभी गोठ पानी लेने तो कभी -“भ्यारपन को एगो देख ढैय् जरा” (बाहर कौन आ गया, देखना) कहकर इधर-उधर भेजती रहती थीं. हम भी “चट-चट” (तुरंत) जाते और फिर वहीं बैठ जाते थे.
 वहाँ बैठे रहने का हमारा एक लालची ‘मोटिव’ होता था. वह लालची मोटिव ‘नॉणी’ (मक्खन) खाने का था. ईजा छाँ फ़ानने के बाद ‘नॉणी’ निकाल कर ‘काठ’ के बर्तन में रख देती थीं. उसके बाद तीन बार छाँ के छींटे इधर -उधर को मारती थीं. ईजा कुछ भी करे लेकिन हमारी नज़र नॉणी पर ही होती थी. उसके बाद ईजा थोड़ी-थोड़ी नॉणी निकालकर हम सारे भाई-बहनों के हाथ में रख देती थीं. हम एक बार में ही उसे चट कर जाते और फिर हाथ आगे कर देते थे. ईजा कहती थीं-“सब तिकें दी दुँ” (सब तुम्हें ही दे दूँ?). यह कहते हुए ईजा एक बार फिर थोड़ा नॉणी हाथ में रख देती थीं और बोलतीं- “जा अब पन्हा, मैंकें काम कन ढैय्” (अब उधर जाओ, मुझे काम करने दो). हम चट उठकर गोठ जाते और गिलास लेकर वहाँ फिर खड़े हो जाते थे.
वहाँ बैठे रहने का हमारा एक लालची ‘मोटिव’ होता था. वह लालची मोटिव ‘नॉणी’ (मक्खन) खाने का था. ईजा छाँ फ़ानने के बाद ‘नॉणी’ निकाल कर ‘काठ’ के बर्तन में रख देती थीं. उसके बाद तीन बार छाँ के छींटे इधर -उधर को मारती थीं. ईजा कुछ भी करे लेकिन हमारी नज़र नॉणी पर ही होती थी. उसके बाद ईजा थोड़ी-थोड़ी नॉणी निकालकर हम सारे भाई-बहनों के हाथ में रख देती थीं. हम एक बार में ही उसे चट कर जाते और फिर हाथ आगे कर देते थे. ईजा कहती थीं-“सब तिकें दी दुँ” (सब तुम्हें ही दे दूँ?). यह कहते हुए ईजा एक बार फिर थोड़ा नॉणी हाथ में रख देती थीं और बोलतीं- “जा अब पन्हा, मैंकें काम कन ढैय्” (अब उधर जाओ, मुझे काम करने दो). हम चट उठकर गोठ जाते और गिलास लेकर वहाँ फिर खड़े हो जाते थे.
ईजा हमको ताजी छाँ देती थीं तो हम दो-तीन गिलास पी जाते थे. छाँ खत्म होने पर खाली गिलास में जोर का ‘सुड़ूक’ (खाली गिलास से आवाज निकालते) मारते थे. ईजा बीच में पूछ लेती थीं- “खटि नि है रे”, नतर लूण धर ले’ (खट्टी तो नहीं हो रही है, नहीं तो नमक रख ले). हम तुरंत बोलते-“ईजा भौते बढ़िया है रे” (ईजा बहुत अच्छी हो रही है). उसके बाद ईजा भी एक-दो गिलास छाँ पी लेती थीं.
गाँव में जिनको भी छाँ देनी हो उनको ईजा पहले ही बोल देती थीं- “वो रमेशक ईजा, ब्या हैं छाँ लिजया हां” (ओ रमेश की मम्मी, शाम को छाँछ ले जाना). परन्तु कुछ लोगों को हम देने जाते थे. ईजा छाँ फानने के बाद कहतीं- “च्यला एक कमण्डली छाँ जरा पार आमकें दी हाँ ढैय् , उन ले झोई बने लिल” (बेटा एक डोलची छाँछ सामने वाली दादी को दे आ, वो भी कढ़ी बना लेंगे). हम ‘बाखे’ (एक साथ कुछ घर) जाने के लिए तो हमेशा तैयार रहते थे. बस कोई बहाना मिल जाए…
ईजा आज भी छाँ फानते हुए हमें याद करती हैं. गाँव में आज भी छाँ बांटी जाती है लेकिन अब झोई-भात कभी-कभी ही बनता है. अब ईजा खुद ही गिलास लाकर छाँ पीती हैं और तय करती हैं कि ‘छाँ खट्टी है कि नहीं”….
जिस दिन ईजा छाँ फानती थीं, उस दिन तो ‘झोई’ (कढ़ी) बनती ही थी. उसके एक-दो दिन आगे तक भी बनती रहती थी. लगभग रोज-रोज झोई -भात खाकर ‘बिछन’ (मन भर जाना ) हो जाती थी. ईजा से कहते भी थे कि रोज-रोज झोई…आगे कुछ बोलने से पहले ही ईजा का पेटेंट जवाब आ जाता था- मैसुंकें मिलण नि में, म्यर च्यल-च्येलियों के बिछन हेगे”( लोगों को मिल नहीं रही है, मेरे बच्चों का मन भर गया). इस बात को हम लगभग रोज ही सुनते और फिर सपोड़ा-सपोड़, झोई-भात खाने लग जाते थे.
ईजा आज भी छाँ फानते हुए हमें याद करती हैं. गाँव में आज भी छाँ बांटी जाती है लेकिन अब झोई-भात कभी-कभी ही बनता है. अब ईजा खुद ही गिलास लाकर छाँ पीती हैं और तय करती हैं कि ‘छाँ खट्टी है कि नहीं”…. कभी -कभी तो छाँ फ़ानने के बाद कुछ समय तक सोच में पड़ जाती हैं क्योंकि हम अब “अमूल बटर” वाले हो गए हैं…
(थू..थू…थू .. हाक झन लागो)
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पहाड़ के सवालों को लेकर मुखर रहते हैं।)