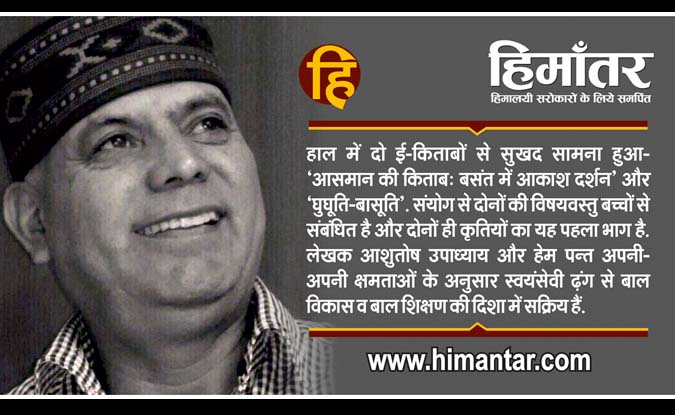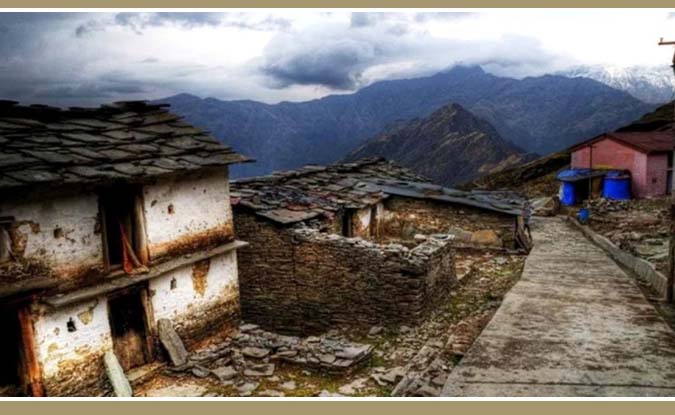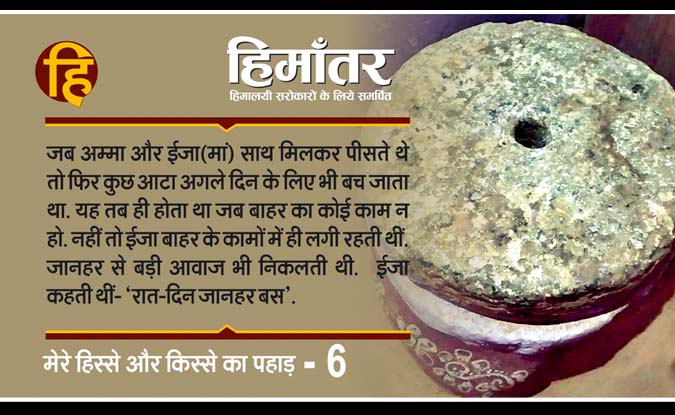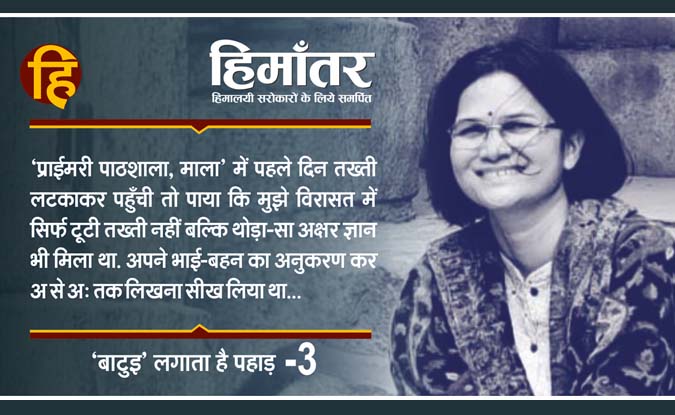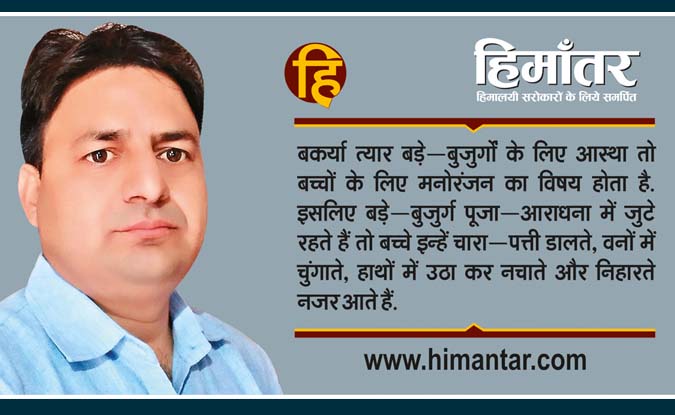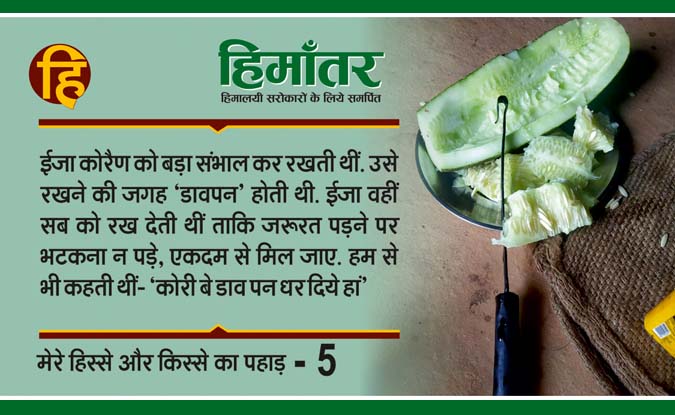लॉक डाउन से पहले मिले बड़े लेखक का बड़ा इंटरव्यू
ललित फुलारा
धैर्य से पढ़ना पिछली बार हिमांतर पर आपने 'ईमानदार समीक्षा' पढ़ी होगी. अब वक्त है 'बड़े लेखक' का साक्षात्कार पढ़ने का. लेखक बहुत बड़े हैं. धैर्य से पढ़ना. लेखक बिरादरी की बात है. तीन-चार पुरस्कार झटक चुके हैं. राजनीतिज्ञों के बीच ठीक-ठाक धाक है. सोशल मीडिया पर चेलो-चपाटों की भरमार. संपादकों से ठसक वाली सेटिंग. महिला लेखिकाओं के बीच लोकप्रियता चरम पर. विश्वविद्यालयों में क्षेत्र और जात वाला तार जुड़ा हुआ है. कई संगठनों का समर्थन अलग से. अकादमी से लेकर समीक्षकों तक फुल पैठ. पूरी फौज है. बौद्धिक टिप्पणी के लिए अलग. गाली-गलौच के लिए छठे हुए. सेल्फी और शेयरिंग के लिए खोजे हुए. फिजिकल अटैक के लिए कभी-कभार वाले. साक्षात्कारकर्ता से टकरा गए थे किसी रोज लॉकडाउन से पहले. मार्च का महीना था. गले में गमछा और हाथ में किताबें लिए सरपंच बने फिर रहे थे. थोड़ी-सी नोंकझोक के बाद ऐसी दोस्ती हुई ...