‘बाटुइ’ लगाता है पहाड़, भाग—7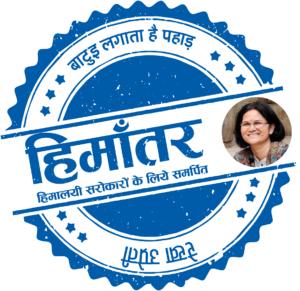
- रेखा उप्रेती
‘रत्याली’ मतलब रात भर चलने वाला गीत, नृत्य और स्वाँग. लड़के की बरात में नहीं जाती थीं तब महिलाएँ. साँझ होते ही गाँव भर की इकट्ठी हो जातीं दूल्हे के घर और फिर घर का चाख बन जाता रंगमंच… ढोलकी बजाने वाली बोजी बैठती बीच में और बाकी सब उसे घेर कर…
दूल्हे की ईजा अपना ‘रंग्याली पिछौड़ा’ कमर में खौंस, झुक-झुक कर सबको पिठ्या-अक्षत लगाती … नाक पर झूलती बड़ी-सी नथ के नगीने लैम्प की रौशनी में झिलमिलाते रहते. बड़ी-बूढ़ियाँ उसे असीसती, संगिनियाँ ठिठोली करतीं तो चेहरा और दमक उठता बर की ईजा का… सबको नेग भी मिलता, जिसे हम ‘दुण-आँचोव’ कहते…
शगुन आँखर देकर ‘गिदारियाँ’ मंच खाली कर देतीं और विविध चरणों में नाट्य-कर्म आगे बढ़ने लगता. कुछ देर गीतों की महफ़िल जमती, फिर नृत्य का दौर शुरू होता… नाचना अपनी मर्ज़ी पर नहीं बल्कि दूसरों के आदेश पर निर्भर करता. ‘आब तू उठ’ कहकर जिसकी ओर इशारा कर दिया जाता उसे दोनों पैरों में घुँघरू बाँधने ही पड़ते…
हमारी अम्मा “सुन री सखी मोहे साजना बुलाए…” पर धीमे-धीमे कदम चलाती. जया दी उठतीं तो “चली कौन से देस गुजरिया” गूँजने लगता. जी हाँ, फ़िल्मी गीत भी होते थे अक्सर … पर गाए अपनी ही ‘लहक’ में जाते थे, ढोलक मंजीरा और घुँघरू की ताल पर… ‘बोल तुम्हारे लय हमारी’ वाले अंदाज़ में सनीमा वालों को टक्कर देतीं थीं सब…
नाच के गीत सबके तय होते. नृत्यांगना के उठकर पैर ‘झंकाते’ ही उसका गीत भी उठ जाता. कोई सिर्फ़ खड़ी ढोलकी की थाप पर थिरकता, किसी से लिए पहाड़ी गीत गाया जाता. हमारी अम्मा “सुन री सखी मोहे साजना बुलाए…” पर धीमे-धीमे कदम चलाती. जया दी उठतीं तो “चली कौन से देस गुजरिया” गूँजने लगता. जी हाँ, फ़िल्मी गीत भी होते थे अक्सर … पर गाए अपनी ही ‘लहक’ में जाते थे, ढोलक मंजीरा और घुँघरू की ताल पर… ‘बोल तुम्हारे लय हमारी’ वाले अंदाज़ में सनीमा वालों को टक्कर देतीं थीं सब… अल्मोड़ा वाली चाची “ मोहे पनघट पे नंदलाल …” पर आँचल सँवार नाच शुरू करती तो हमारी साँसे रुक जातीं. एक तो इतनी सुन्दर थीं वे, गला भी मीठे सुर से सधा हुआ …

इस बीच किसी आमा को याद आता- “ अरे, दिया भी देख लो रे!”
तांबे की तौली में दो दिए जलाकर रखे जाते रात भर, जो “बर और ब्योलि’ के प्रतिरूप होते… उनका अकम्पित जलना इस बात का प्रमाण होता कि लड़की वालों के घर में विवाह की मांगलिक रस्में ठीक चल रही हैं. सम्प्रेषण के साधन नहीं थे तब. बरात पहुँची या नहीं, दूल्हा-दुल्हन खुश हैं या नहीं, विवाह निर्विघ्न हो रहा है या नहीं … सब सन्देश इन दियों की रोशनी से पढ़ लेतीं वे. दियों की जगमगाहट देखकर आने वाली काखी सबको सूचित करती कि ‘बर’ ज्यादा प्रसन्न है या ‘ब्योलि’ ज्यादा खुश दिख रही है.
“मी नी मानुलS तेSरी बात, चाहे सासू कस्स कर..” गाते हुए वे सासुओं के समुदाय को खूब खरी-खोटी सुना डालतीं. इन स्वांगों में उनका निश्छल स्वभाव, उन्मुक्त उमंगें, दबी हुई इच्छाएँ और कुंठाएँ, अनकहे दर्द और शिकायतें सब व्यक्त हो जाते…

आधी रात के बाद शुरू होते स्वाँग. पहाड़ की सीधी सरल मेहनतकश नारी का यह अलग अवतार होता. कोई अपने देवर के कपड़ों में सजधज कर अवतरित होता, कोई ससुर के बाने से सजा तो कोई पड़ोस के बड़बाज्यू का रूप धरकर … और फिर वाचिक, कायिक, आहार्य… हर तरह का अभिनय साकार हो उठता. ढोलक मंजीरे वालियाँ पीछे सरक जातीं, गीत गाती मंडली दर्शकों में तब्दील हो जातीं. हम बच्चे कौतुहल से देखते रह जाते …उन्हें हमेशा गोठ-भितेर, आँगन-बाड़-ख्वाड़, धुर-धार, खेत-बगड़ में खटते देखने की आदी थीं आँखें… यह रूपांतरण अद्भुत लगता. उनकी हर अदा, हर नक़ल, हर संवाद पर कहकहे लगते, एक-दूसरे की पीठ पर धौल जमते, पूरा चाख खिलखिला उठता…
“तदुक छलछलाट नि करो रे!!” (इतनी छलछलाहट मत करो) कोई सास बनावटी क्रोध दिखाकर बहुओं को बरजती….पर उनकी कौन सुने आज?
“मी नी मानुलS तेSरी बात, चाहे सासू कस्स कर..” गाते हुए वे सासुओं के समुदाय को खूब खरी-खोटी सुना डालतीं. इन स्वांगों में उनका निश्छल स्वभाव, उन्मुक्त उमंगें, दबी हुई इच्छाएँ और कुंठाएँ, अनकहे दर्द और शिकायतें सब व्यक्त हो जाते… उनकी प्रतिभाएँ भी… जो प्राय: घास, पिरूव, पुआल और लकड़ी के गट्ठरों, पानी की कसेरी-गगरियों, मोल (खाद) भरी डलियों के नीचे हाँफते रहने को विवश थी.
स्वाँग का दूसरा नज़ारा मिलता होलियों में. होलियाँ कुमाऊँ में खेली नहीं गाई जाती है और वह भी महीने भर तक… पुरुष रात को आग जलाकर होली की बैठक लगाते और स्त्रियाँ दिन में … बारी-बारी सबके आँगन में होलियाँ गायीं जाती और खूब स्वाँग लगते…
हमारी ठुलि बुब यानी बड़ी बुआ इस कला में सिद्धहस्त थीं. गाँव या रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका ठाठ् बुआ न लगाती हों. बुआ जब भी आतीं, सब उन्हें घेर कर बैठ जाते. उनका ‘ठाठ्’ देखने के लिए किसी स्थान या अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वे कभी भी, कहीं भी शुरू हो जातीं
स्वाँग का ही एक और रूप था जिसे ‘ठाठ्’ कहते. स्वाँग में जहाँ वेशभूषा महत्वपूर्ण होती वहाँ ‘ठाठ्’ में कोई तामझाम नहीं होता था. बस किसी व्यक्ति के हाव-भाव (जिसे हम लट्टैक कहते) और बोलने के ढंग का अनुकरण करने की प्रतिभा अपेक्षित होती. हमारी ठुलि बुब यानी बड़ी बुआ इस कला में सिद्धहस्त थीं. गाँव या रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका ठाठ् बुआ न लगाती हों. बुआ जब भी आतीं, सब उन्हें घेर कर बैठ जाते. उनका ‘ठाठ्’ देखने के लिए किसी स्थान या अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वे कभी भी, कहीं भी शुरू हो जातीं और वहीं रंगमंच धड़कने लगता …

बड़ी बुआ अब बुजुर्ग हो गयीं हैं, वर्षों से मिलना भी नहीं हुआ.. पर खबर मिलती रहती है कि उनकी कला अभी जवान है और जिंदादिली भी…
(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के इन्द्रप्रस्थ कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं)


आहा भौतै सुंदर। साकार हैग्यो पहाड़।