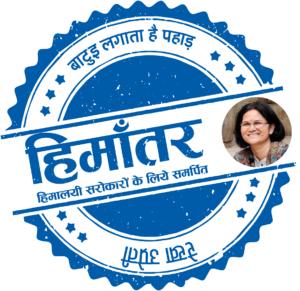‘बाटुइ’ लगाता है पहाड़, भाग—16
- रेखा उप्रेती
कुछ अजीब-सा शीर्षक है न…
नहीं, यह कोई मुहावरा नहीं, एक दृश्य है जो कभी-कभी स्मृतियों की संदूकची से बाहर झाँकता है… पीतल की करछी में कोयले का अंगार ले जाती रघु की ईजा… जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाती… अपने घर की ओर जाती ढलान पर उतर रही है, बहुत सम्हल कर… कि करछी से अंगार गिरे भी नहीं और बुझे भी नहीं. चूल्हा कैसे जलेगा वरना…
तीस-चालीस साल पहले जो पहाड़ में रह चुके हैं या बचपन पहाड़ों में बिताया है, उनके लिए यह दृश्य अपरिचित नहीं होगा. चूल्हे में आग बचाकर रखना या ज़रुरत पड़ने पर दूसरे घरों से आग जलाने के लिए जलता कोयला ले जाना, उस वक़्त की ज़रुरत भी थी और सीमित संसाधनों के बीच एक ऐसी जीवन-शैली का उदाहरण भी, जहाँ मामूली से मामूली वस्तु भी ‘यूज़ एंड थ्रो’ की ‘कैटेगरी’ में नहीं थी.
मुझे याद है सुबह का भोजन बन जाने के बाद अधजली लकड़ियों को बुझा कर अलग रख दिया जाता और हलकी सी राख की परत में लिपटे अंगारे चिमटे से उठाकर सगड़ में डाल दिए जाते. सगड़ में राख भरी रहती और उसी में दहकते हुए अंगारे दबा दिए जाते थे. दोपहर या साँझ की चाय का समय हो तो इन्हीं अंगारों से राख की परत हटाकर, फूँक मारते हुए छिलुक जला दिया जाता और फिर चूल्हे की लकड़ियाँ सुलगा दी जातीं.

जाड़ों की रात इसी सगड़ को तापते हुए किस्से-कहानियों के दौर भी चला करते..
सगड़ की वह राख भी “अयसी-वयसी’ नहीं बड़े काम की चीज़ थी. एकदम मखमली मुलायम… दो-चार दाने आलू उसमें दबा कर छोड़ दीजिए तो बढ़िया स्नैक्स तैयार… . भात और दाल पकाने के बर्तन यानी तौली और भड्डू इसी राख में पुतकर चूल्हे पर चढ़ने की योग्यता अर्जित करते. इससे उनकी कलई भी बची रहती और बाद में माँजना भी सहज रहता. घर-भर के बर्तन इसी राख से मँजते-सँवरते… बिना ‘बिम-बार’ के भी ऐसी चमकार मारते वे पीलत काँसे के भारी-भरकम बर्तन कि टी.वी. के सारे विज्ञापन उनके आगे पानी भरें. बाड़े में उगी पत्तेदार हरी सब्जियों पर बुरक दीजिए वह राख, कीटनाशक की ज़रुरत ही नहीं पड़ती थी कभी. और हाँ कोई छोटा-मोटा ‘लोकल’ भूत लग जाए आपको तो किसी बड़बाज्यू से इसका भभूत लगवा लीजिए.
इस काम में हमारे बड़बाज्यू सिद्धहस्त थे… हमारी कई छोटी-बड़ी बीमारियों का एक ही रामबाण इलाज था… साँझ के समय बड़बाज्यू चुटकी भर राख़ उठाते, हथेली में रख उँगलियाँ घुमाते हुए कुछ बुदबुदाते फिर चुटकी से हमारे माथे पर उसे लगाते हुए ज़ोर से हाक छोड़ते… हम सिहर उठते और सचमुच खुद को हल्का महसूस करते और फिर ठीक भी हो जाते… डॉक्टर और दवाई का नाम ही सुना होता बस…
सगड़ की इसी राख के बीच से सुबह-सुबह एक कोयला उठा हम दाँतों को रगड़ लेते. ना ब्रश की ज़रुरत न पेस्ट की. दाँतों की चमक तो बरकरार रहती ही, मजबूती ऐसी की अखरोट दाँतों से तोड़ लेते थे. अखरोट के छिलके भी दाँतों के बड़े काम आते. उन्हें जलाकर पाउडर बना लीजिए और मंजन की तरह इस्तेमाल कीजिए. आम के आम गुठलियों के दाम …
वैसे यह मुहावरा मुझे कुछ असंगत-सा लगता है. कभी देखा है किसी ने गुठलियों के दाम मिलते हुए? पर अब चल पड़ा है तो क्या कीजे? यूँ भी फलों का राजा ठहरा …. कौन पंगा ले!! पर अपने पहाड़ में देखा है कितने ही फल और पेड़ इस उपाधि के असली हक़दार हैं….
ठांगर में चढ़ी इसकी खूबसूरत झाल पर जब नन्हे-नन्हे फुल्यूड़ आते हैं न, तो इतने दिलकश लगते हैं कि लोकगीतों में नायिका की सुन्दरता का बखान करते हुए उसकी उपमा दी जाती है. युवा होने पर इस काकड़ को लम्बाई में चीरकर उसमें पिसा हुआ नमक लगाकर खाइए और स्वाद में गोते लगाइए. पिसा हुआ नमक भी पहाड़ की अपनी विशिष्ट ‘डेलीगेसी’ है.
पहाड़ी ‘काकड़’ को ही लीजिए. कुदरत की बहु-उपयोगी नेमत…
ठांगर में चढ़ी इसकी खूबसूरत झाल पर जब नन्हे-नन्हे फुल्यूड़ आते हैं न, तो इतने दिलकश लगते हैं कि लोकगीतों में नायिका की सुन्दरता का बखान करते हुए उसकी उपमा दी जाती है. युवा होने पर इस काकड़ को लम्बाई में चीरकर उसमें पिसा हुआ नमक लगाकर खाइए और स्वाद में गोते लगाइए. पिसा हुआ नमक भी पहाड़ की अपनी विशिष्ट ‘डेलीगेसी’ है. नमक की डलियों को सिलबट्टे पर हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, अलसी या भंगीरे के बीजों के साथ पीस कर रख लिया जाता हैं. चूल्हे में सिकी गेंहू की गुदगुदी या मड़ुए की करारी रोटी में जरा सा घी चुपड़, इस ‘पीसी नूण’ के साथ रोल बनाकर खाइए, भट या छाँछ के जौल में मिलाइए, आलूबुखारे में छिड़क लीजिए या पहाड़ी नींबू के साथ सान कर आनंद लीजिए…
हाँ तो इस काकड़ का एक उपयोग ‘रैत’ यानी रायते के रूप में भी किया जाता. ककड़ी का करारापन राई के तीखेपन से गठजोड़ कर गजब का फ्लेवर अख्तियार कर लेता है. राई भी ऐसी तीखी कि सीधे ‘बरमांड’ यानि मस्तिष्क में पहुँचकर उसकी शिराओं को झंकृत कर दे… पितृ-पक्ष में दाल-भात-टपकी, बड़े-पूरी-खीर और खटाई के साथ-साथ यह रायता न बने तो पहाड़ के पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती…

काकड़ के पूरी तरह पक कर खूब गदबदे, गहरे पीले हो जाने पर उसे कोर, पीसी हुई उड़द दाल में मिलाकर, बड़ियाँ बना, सुखाकर पूरे साल के लिए रख ली जातीं. ककड़ी निचोड़कर जो पानी निकलता, उसमें रात भर धान भिगोकर सुबह चिवड़े कूटे जाते… छिलके गाय-बछिया के काम आते और बीज सुखाकर रख लिए जाते कि अगले साल फिर से काकड़ की झाल उगाई जा सके. हुए न आम के आम…
यह तो मात्र एक अदना-सा उदाहरण है कि चीजों को बरता कैसे जाता था तब… कई अंशों में अब भी… कोई भी वस्तु फेंक देने का रिवाज़ नहीं. चीड़ की झड़ी हुई बारीक-बारीक पत्तियाँ तक बहु उपयोगी … जंगल से समेट कर लाई जातीं, जानवरों के छा’न में बिछती, उन्हें इससे गर्माहट मिलती और हमें मिलती खेतों के लिए जैविक खाद… हरी पत्तेदार या मूली कद्दू जैसी मौसमी सब्जियाँ सुखाकर स्टोर कर ली जातीं.. नमक के संदर्भ में हमें विशेष हिदायत थी कि वह जमीन पर नहीं गिरना चाहिए क्योंकि जो नमक को गिराएगा बाद में उसे अपनी पलकों से नमक के कण उठाने पड़ेंगे… हमने देखा था धान सुखाते या कूटकर समेटते हुए आँगन के पत्थरों के बीच की दरारों में फँस गए दानों को आमा एक-एक कर निकालती… मेरी माँ हमेशा समझाती कि अन्न का दाना दरवाजे के कोने में पड़ा हो तब भी आस में रहता है कि मुझे उठा लिया जाएगा, वहाँ से बाहर फेंक दें तो फिर श्राप फोकता है…
रिड्यूस, री-यूज़, री-साइकिल जैसी अवधारणाएँ तो बाद में बनीं, हमने तो अनुभव से जाना था कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए… अब तो हम भी कूड़े का उत्पादन करने में माहिर हो चुके हैं पर हमारी समृद्ध बोली में कूड़े-कचरे के लिए कोई शब्द नहीं था … दिल्ली आने से पहले हमने न कूड़े के ढेर देखे थे न नालियों में बहता दुर्गंधयुक्त पानी…
अन्न की कीमत वही जान सकता है न जो उसे उगाने में खून-पसीना एक करता हो. अनाप-सनाप कमाई से अन्न खरीदने वाला कैसे सोच सकता है ऐसी मार्मिक बात…
रिड्यूस, री-यूज़, री-साइकिल जैसी अवधारणाएँ तो बाद में बनीं, हमने तो अनुभव से जाना था कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए… अब तो हम भी कूड़े का उत्पादन करने में माहिर हो चुके हैं पर हमारी समृद्ध बोली में कूड़े-कचरे के लिए कोई शब्द नहीं था … दिल्ली आने से पहले हमने न कूड़े के ढेर देखे थे न नालियों में बहता दुर्गंधयुक्त पानी…
पर यह दशकों पहले कि बात है, अब तो पहाड़ भी सभ्य होने लगे हैं…
(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के इन्द्रप्रस्थ कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं)