
हम याद करते हैं पहाड़ को… या हमारे भीतर बसा पहाड़ हमें पुकारता है बार-बार? नराई दोनों को लगती है न! तो मुझे भी जब तब ‘समझता’ है पहाड़ … बाटुइ लगाता है…. और फिर अनेक असम्बद्ध से दृश्य-बिम्ब उभरने लगते हैं आँखों में… उन्हीं बिम्बों में बचपन को खोजती मैं फिर-फिर पहुँच जाती हूँ अपने पहाड़… रेखा उप्रेती दिल्ली विश्वविद्यालय, इन्द्रप्रस्थ कॉलेज के हिंदी विभाग में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं. प्रस्तुत है रेखा उप्रेती द्वारा लिखित ‘बाटुइ’ लगाता है पहाड़ की 9वीं सीरीज…
‘बाटुइ’ लगाता है पहाड़, भाग—9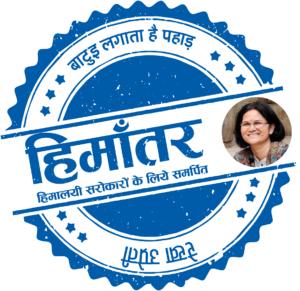
- रेखा उप्रेती
परीक्षाएँ तो हमने भी बहुत दीं, पर तब न नंबरों का पारा ऐसे चढ़ता था, न माँ-बाप हमें सूली पर चढ़ाकर रखते थे. हमारे बाबूजी ने एक कंडीशन ज़रूर रखी हुई थी कि जो फेल होगा उसे आगे नहीं पढ़ाएँगे. इस विषय में बाबूजी कितने गंभीर थे मालूम नहीं क्योंकि किसी भाई-बहन ने कभी फ़ेल होने की हिमाक़त नहीं की. हाँ, मैं ज़रूर एक बार फ़ेल होते होते बची…
किस्सा 1977 का है. मैं पाँचवीं कक्षा में थी. नवम्बर का महीना ….रोज़ की तरह जब मैं स्कूल से लौटी तो बाबूजी घर पर मिले. मैं खुशी से उछलने को हुई मगर माँ और दीदी की हड़बड़ाई-सी स्थिति देख असमंजस में पड़ गयी. साल में एक बार दिल्ली से ‘घर’ आने वाले बाबूजी का यूं बगैर कोई इत्तिला दिए चले आना हैरानी की बात तो थी… पर ये हड़बड़ी….!!
संक्षेप में कहानी यह थी कि ठीक सात दिन बाद मेरी मँझली दीदी की शादी का मुहूर्त निकल आया था और हमें अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना हो जाना था. कोई चार-छः महीने पहले दीदी के भावी श्वसुर हमारे यहाँ ठहरकर और गाँव भर से ‘अच्छा परिवार’ होने का प्रमाणपत्र लेकर गए थे. अब पिताजी यह खबर लेकर आए हैं कि अगले सप्ताह शादी है. सारी तैयारियाँ करनी हैं. सारा कारोबार समेटो और दिल्ली चलो… जल्दी-बाजी में किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे स्कूल में सूचना ही दे देते या छुट्टी का प्रार्थना-पत्र ही लिख कर भेज देते.
पहाड़ी गाँव के खुले-खिले खूबसूरत परिवेश के मुकाबले दिल्ली की यह घिच-पिच दुनिया आकर्षक तो बिलकुल नहीं थी पर दिलचस्प ज़रूर थी… सटे-सटे पीले मकान, तंग गलियाँ, कूड़े-करकट के ढेर, भीड़-भड़क्का… हरी-भरी सुन्दर पहाड़ियाँ तो दूर की बात, आसमान देखने के लिए भी गर्दन उठानी पड़ती…
तो हम दिल्ली चले आए. सात दिन बाद दीदी की शादी हो गयी. पर हम गाँव नहीं लौटे…
भाई बाबूजी के साथ दिल्ली में रहकर पढ़ रहे थे. दो दीदियाँ भी दिल्ली की हो गयीं. अब वापस गाँव लौटने का कोई ‘मकसद’ नहीं रह गया था. मेरा स्कूल तो छूट ही चुका था…

अगले चार महीने मैंने भी एक नयी किस्म की दुनिया को ‘एक्सप्लोर’ किया. पहाड़ी गाँव के खुले-खिले खूबसूरत परिवेश के मुकाबले दिल्ली की यह घिच-पिच दुनिया आकर्षक तो बिलकुल नहीं थी पर दिलचस्प ज़रूर थी… सटे-सटे पीले मकान, तंग गलियाँ, कूड़े-करकट के ढेर, भीड़-भड़क्का… हरी-भरी सुन्दर पहाड़ियाँ तो दूर की बात, आसमान देखने के लिए भी गर्दन उठानी पड़ती… गाँव की हमारी दुबली-पतली, पर एकदम चुस्त-दुरुस्त ‘आमा’ की जगह यहाँ हमारी मकान मालकिन ‘बेजी’ थीं, चकाचक सफ़ेद सलवार कमीज और दुपट्टे में लिपटी दिन भर खाट पर ठाट से पसरी रहती. उनके बड़े से मकान में बहुत-सी खोलीनुमा कोठरियाँ थीं. हर कोठरी में एक परिवार बसता.. हर परिवार में दो-तीन बच्चे होते. स्कूल से लौटकर बच्चों की टोली गली में जमा होती और तरह-तरह के खेलों में मशगूल हो जाती… मैं भी धीरे-धीरे उस टोली का हिस्सा बन गयी. चील-चील काटा…पोशम्पा भई पोशम्पा… ऊँच-नीच का पापड़ा… छुपम-छुपाई… विष-अमृत…. पकड़म-पकड़ाई…. गिल्ली-डंडा… स्टापू… लंगडी टांग… कंचे, पिठ्ठू ….और भी जाने कितनी तरह के खेल लगातार चलते रहते…. किसी किसी दिन मेरा भाई मुझे नई जगहों पर ले जाता. हमारे घर से काफ़ी दूर यमुना पर लोहे का पुल था, उसके ऊपर से रेल गुजरती तो पुल का थरथराना हमें रोमांचित करता … तांगे की सवारी जब पुल पार करती तो घोड़े के पैरों की टकटकाहट देर तक हवा में गूँजती रहती… एक बार किसी को बिना बताए हम रेल की पटरी देखने भी गए. कई गलियाँ पार कर पुश्ते पर चढ़कर हम पटरी तक पहुँचे थे…. इतवार के दिन यमुना पर बने नावों के पुल को पार कर हम विजय घाट या शान्ति-वन जा पहुँचते. हरी घास पर चक्कर लगाते पानी के फव्वारों के साथ-साथ भागते . ढलानों पर लेटकर लुड़कते हुए नीचे आते… ताल पर तैरती बत्तखों को मूँगफली खिलाते…. वापसी पर नावों के हिलते पुल के किनारे खड़े ठेले पर ताज़ा गन्ने का रस पीते… रात को अँगीठी की आँच पर शकरकंद भूनी जाती और रेडियो पर ‘हवामहल’ और ‘छायागीत’ सुनते-सुनते हम सो जाते … ज़िंदगी खूब मज़े में गुज़र रही थी…
हाँ, हर सुबह गली भर के बच्चों को स्कूल जाते देख उदासी ज़रूर घिर आती.
फिर हुआ यूं कि नवीन दा की शादी के सिलसिले में हम वापस गाँव पहुँच गए. विवाह की धूमधाम के बाद मार्च का पहला हफ़्ता … हमें वापस दिल्ली लौटना था, मन में गहरी उदासी थी, पर तभी कुछ और घटना हुई…
“अगर आप चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं कि आपकी बिटिया भी परीक्षा में बैठ सके” मास्साब ने बाबूजी से कहा. जाने क्या सोचकर बाबूजी ने झट से हामी भर दी. यह भी नहीं सोचा कि चार महीने से जिसने ‘मसि कागद छूयो नहीं, कलम गहि नहीं हाथ…’ वह लड़की बोर्ड की परीक्षा में बैठकर करेगी क्या!!
लौटने से एक दिन पहले हम मंदिर जा रहे थे. मंदिर से सटा हुआ हमारा स्कूल था. स्कूल खुला था, बाहर कक्षाएँ चल रही थी. मैं वहीं अटक गयी. झिझकते हुए अध्यापकों को नमस्ते की…सहपाठियों से मिली. गाँव का यह स्कूल प्राइमरी तक ही था. अत: पाँचवीं पास कर बड़े स्कूल में जाने के लिए भी बोर्ड की परीक्षा ली जाती थी. बोर्ड के परीक्षार्थियों के फार्म भरे जा चुके थे. मेरा नाम उनमें नहीं था… मैं और उदास हो गयी..
“अगर आप चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं कि आपकी बिटिया भी परीक्षा में बैठ सके” मास्साब ने बाबूजी से कहा. जाने क्या सोचकर बाबूजी ने झट से हामी भर दी. यह भी नहीं सोचा कि चार महीने से जिसने ‘मसि कागद छूयो नहीं, कलम गहि नहीं हाथ…’ वह लड़की बोर्ड की परीक्षा में बैठकर करेगी क्या!!

तो माँ के साथ मैं गाँव में रुक गयी, दीदी और भाई बाबूजी के साथ दिल्ली लौट गए. परीक्षा में कुछ ही दिन बचे थे. क्या विषय थे, कैसे और क्या पढ़ा, अब कुछ भी याद नहीं पर वह दिन अच्छी तरह याद है जिस दिन परीक्षा होनी थी. जी हाँ, सारे विषयों की परीक्षा एक ही दिन थी. गाँव से कोई तीन-चार किलोमीटर दूर एक बड़ा स्कूल था. इलाके भर के सभी प्राइमरी स्कूलों के लिए वही परीक्षा सेंटर था…
ऊँची-नीची पहाड़ियों पर चढ़ते-उतरते, खेतों की पगडंडियों पर सम्हल-सम्हल चलते, चप्पल हाथ में लेकर गाड़-गधेरों को पार करते हम परीक्षा-भवन में पहुँचे. कुछ परिचित और बहुत से अपरिचित स्कूली बच्चे वहाँ एकत्रित थे.
सुबह उठी तो सूरज भी अलसाई आँखें मलता हुआ जाग रहा था. चाची के गोठ में चूल्हा सुलगाए माँ मेरे लिए पराँठे बना रही थी. पता चला कि हमारे चूल्हे के भीतर रात बिल्ली ने नन्हे-नन्हे बच्चे दिए थे. “अच्छा शगुन है..” चाची ने हँसते हुए कहा. फिर माँ ने माथे पर ‘अक्षत-पिठ्या’ लगाया, चाची ने दही-बतासा खिलाया. एक चवन्नी भी मिली. एक सहेली के कुछ वर्ष बड़े भाई को यह दायित्व सौंपा गया कि वह हमें स्कूल तक छोड़कर आए, हाफ टाइम में पराँठे खिला दे और शाम को वापस घर ले आए.
तो हम वीर सैनालियों की भाँति परीक्षा देने निकले. ऊँची-नीची पहाड़ियों पर चढ़ते-उतरते, खेतों की पगडंडियों पर सम्हल-सम्हल चलते, चप्पल हाथ में लेकर गाड़-गधेरों को पार करते हम परीक्षा-भवन में पहुँचे. कुछ परिचित और बहुत से अपरिचित स्कूली बच्चे वहाँ एकत्रित थे. स्कूल के बड़े से अहाते में हर स्कूल के लिए लाइन से टाट-पट्टियाँ बिछी थीं. सामने बड़ा-सा ब्लेकबोर्ड था. परीक्षा शुरू होने में अभी वक्त था. हम आसपास की झाड़ियों से जंगली फल बटोरने में लगे रहे.
मेरी बुआ जी पास के किसी स्कूल में टीचर थीं. उनकी सहकर्मी ने हमें देखा तो ज़बरन अपने घर ले गयीं. बोली, खाना खाकर जाओ. दो थालियों में दाल-भात-बड़ी की सब्जी परोसकर हमारे सामने रख दिए गए. अब हमसे न तो खाया जाए न मना करने की हिम्मत… किसी तरह ठूँस-ठाँस कर ख़त्म किया और विदा लेकर वापस भागे….
घंटी बजी तो सब दौड़कर अपनी-अपनी जगह पर आ बिराजे. आलथी-पालथी मार कर बैठ गए और घुटने पर गत्ता रखकर लिखाई शुरू कर दी. एक मास्टरजी ने ब्लेकबोर्ड पर प्रश्न लिख दिए थे, जिनके उत्तर हमें अपनी कॉपी पर लिखने थे. एक एक कर सभी विषयों के लिए यही क्रम दोहराया गया. दोपहर हो चुकी थी. पेट में चूहे कूदने लगे थे और चवन्नी भी चुलबुला रही थी. ‘इमली खरीदकर खाएँगे’, यह हमने रास्ते में ही तय कर लिया था.
हाफ टाइम की घंटी बजी तो हमने राहत की साँस ली. स्कूल बाज़ार के बीच में था. भाई ने हमें परांठे के साथ छोले भी खिलाए. खूब छककर खाया . फिर एक दूकान से इमली खरीदी और चटकारे लेते हुए वापस स्कूल की ओर चले. आधी परीक्षा अभी बाकी थी..
मगर बीच में ही हमें रोक लिया गया. मेरी बुआ जी पास के किसी स्कूल में टीचर थीं. उनकी सहकर्मी ने हमें देखा तो ज़बरन अपने घर ले गयीं. बोली, खाना खाकर जाओ. दो थालियों में दाल-भात-बड़ी की सब्जी परोसकर हमारे सामने रख दिए गए. अब हमसे न तो खाया जाए न मना करने की हिम्मत… किसी तरह ठूँस-ठाँस कर ख़त्म किया और विदा लेकर वापस भागे…. अगली परीक्षा शुरू हो चुकी थी. झट से प्रश्न उतार हमने भी भागीदारी निभाई. शाम होते होते सारे विषय निबटा दिए गए और हम खुशी-खुशी घर लौट आए.

जिस दिन रिज़ल्ट आना था, माँ बाज़ार सौदा लेने गयी हुई थी. लौटते हुए गाँव की सीमा पर किसी ने उन्हें खबर दी स्कूल का रिज़ल्ट आ गया. “कैसा रहा?” डरते-डरते माँ ने पूछा.
“दो बच्चे फ़ेल हुए हैं, बाकी पास है” उत्तर मिला. माँ ने मन ही मन सोचा, “एक तो मेरी लड़की होगी, दूसरा पता नहीं कौन फेल हो गया..!!”
कुछ दिनों बाद हमें बाबूजी की चिठ्ठी मिली. कुशल-मंगल पूछने के बाद लिखा था, …बिटिया का साल तो बर्बाद हो ही गया, इस साल कैसे पास होगी…..
मेरे पास होने की चिठ्ठी तब तक उनके पास नहीं पहुँची थी….
तो ऐसे भी हो जाते थे इम्तिहान में पास ….कितना अच्छा होता अगर ज़िंदगी के सारे इम्तिहान यूं ही मज़े-मज़े में निबट जाते और बोर्ड परीक्षाओं का ‘मसाण’ सर पर न सवार होता…
(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के इन्द्रप्रस्थ कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं)
