
‘बाटुइ’ लगाता है पहाड़, भाग—14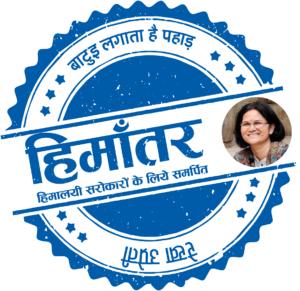
- रेखा उप्रेती
“कल ‘अखोड़ झड़ाई’ है मास्साब, छुट्टी चाहिए.” हमारा मौखिक प्रार्थना-पत्र तत्काल स्वीकृत हो जाता. आखिर पढ़ाई जितनी ही महत्वपूर्ण होती अखोड़ झड़ाई…
गुडेरी गद्ध्यर के पास हमारे दो अखरोट के पेड़ थे, बहुत पुराने और विशालकाय. ‘दांति अखोड़’ यानी जिन्हें दांत से तोड़ा जा सके. दांत से तो नहीं, पर एक चोट पड़ते ही चार फाँक हो जाते और स्वाद अनुपम. गाँव में ‘काठि अखोड’ के बहुत पेड़ थे. काठि माने काठ जैसे, जिन्हें तोड़कर उनकी गिरी निकालना मशक्कत माँगता. अक्सर उन्हें आलपिन से कुरेद कर खाना पड़ता… पर हमारे पेड़ के अखोड़ दांति थे और दूधिया भी.
हम कंटीली झाड़ियों के आस-पास और गधेरे के बहते पानी के नीचे दुबक गए अखरोट खोजकर ऐसे प्रसन्न होते जैसे समंदर से नायब मोती ढूँढ निकाले हों. दोपहर तक यह प्रक्रिया चलती रहती, फिर भारी-भारी डलिया उठाए सब घर की ओर जाती चढ़ाई पर हाँफते हुए चढ़ने लगते….
अखोड़ झड़ाई वाले दिन सुबह-सुबह एक-एक डलिया उठाकर ‘और-पौर’ के सभी बच्चे और बड़े चल पड़ते. दो घरों के साझे पेड़ थे यह. पौर के बड़-बाज्यू जाँठी टेकते हुए आगे-आगे और हम बच्चों की उत्साहित टोली पीछे-पीछे. दोनों पेड़ों पर अखोड़ झाड़ने के लिए नियुक्त एक-एक आदमी रस्सी बाँधकर और एक लम्बी मज़बूत लाठी लेकर चढ़ जाता और दे दनादन अखरोट की बरसात होने लगती. पेड़ों के नीचे समतल मैदान नहीं था, उबड़-खाबड़, जंगली झाड़ियों से भरा इलाका.. तो अखरोट कहाँ-कहाँ गिरे, इसकी पड़ताल चौकन्ने होकर करनी पड़ती. हम कंटीली झाड़ियों के आस-पास और गधेरे के बहते पानी के नीचे दुबक गए अखरोट खोजकर ऐसे प्रसन्न होते जैसे समंदर से नायब मोती ढूँढ निकाले हों. दोपहर तक यह प्रक्रिया चलती रहती, फिर भारी-भारी डलिया उठाए सब घर की ओर जाती चढ़ाई पर हाँफते हुए चढ़ने लगते….

उस दिन छुट्टी के बाद स्कूल के कई साथी गधेरे की ओर रुख करते…. अखरोट ढूँढते हुए उनके बस्ते भी भारी हो जाते…
घर पहुँचकर पौर के आँगन में सारी डलियाँ एक जगह उलट दी जातीं. फिर बँटवारा होता. अखरोट तोड़ने वालों का हिस्सा देकर उन्हें विदा किया जाता और फिर और-पौर के दोनों घरों के बीच बराबर अखरोट बाँटे जाते. चार अखरोट के समूह को ‘चौक’ कहते और उसी हिसाब से बटवारा होता. हम अपना हिस्सा लेकर अपने आँगन में फैला देते…
बाबूजी, चाचाजी, ससुराल की दीदियों, कुछ रिश्तेदारों के लिए अलग रख कर बाँकी अखरोट माँ हमारे बीच बाँट देती. पाँच-छः चौकियाँ हर किसी के हिस्से आतीं और हम अमीर हो जाते. घर के भीतर अपने-अपने ठिकाने बनाकर हम अपनी अमूल्य संपत्ति को रखते और फिर च्यूड़ (घर के बने चिवड़े) के साथ मिलाकर गाल भर लेते…
अखरोट का ‘काठ’ यानी बाहरी मोटा हरा खोल काटकर अलग करना करना पड़ता. माँ और दीदियाँ दातुली (दराती) से खट्ट-खट्ट काटतीं और हम हाथ से उन्हें अलग करते जाते. हमारे हाथ और कपड़े काले रंग में सराबोर हो जाते. इतनी मेहनत से निकला फल हमें भी फलता. बाबूजी, चाचाजी, ससुराल की दीदियों, कुछ रिश्तेदारों के लिए अलग रख कर बाँकी अखरोट माँ हमारे बीच बाँट देती. पाँच-छः चौकियाँ हर किसी के हिस्से आतीं और हम अमीर हो जाते. घर के भीतर अपने-अपने ठिकाने बनाकर हम अपनी अमूल्य संपत्ति को रखते और फिर च्यूड़ (घर के बने चिवड़े) के साथ मिलाकर गाल भर लेते…
सिर्फ़ अखरोट के साथ इतना तामझाम था, बाकी फलों के लिए तो हाथ बढ़ाकर डालियाँ झुकाना और तोड़कर सीधे दांत की कटक लगाना… खुबानी और कुशम्यारु के पेड़ आँगन के आस-पास थे. गर्मियों की छुट्टियाँ इन्हीं के साए में बीततीं. इनकी सघन छाया के नीचे पत्थरों से मकान बनाते हुए खेलते रहते हम… हवाओं से हिलते छोटे-छोटे पत्ते हमारा साथ देते. पत्तियों के बीच खचाखच भरे पीले-नारंगी आभा लिए फल हमें ऊपर बुलाते. हम टहनियाँ पकड़-पकड़ ऊपर चढ़ उनका आमंत्रण स्वीकार करते और खुबानी तोड़-तोड़ खाते… फिर उनकी गुठलियां हमारे खेल में शामिल हो जातीं. खट्टे-मीठे खूब रसीले आल्पखर (आलूबुखारे), लालिमा से भरे मीठे पुलम(प्लम), दूर तक अपनी सुगंध पसारते आडू भी हमारे गहरे दोस्त थे. इनकी डालियाँ हमें गलबहियाँ देकर मिठास से भर देतीं.
नौला, जहाँ से हम पानी भरकर लाते वहाँ नाशपाती का एक बड़ा-सा पेड़ था. उस पेड़ पर गाँव की जिस बुआ का अधिपत्य था वह हमेशा चौकस रहतीं कि उन नाशपतियों पर कोई हाथ न साफ़ कर दे. ऐसा करते देख लें जिसे, उसका नास करने वाली गाली देने को तत्पर … उस पेड़ की नाशपतियाँ ऐसी मीठी और रसीली कि हम अपना नाश करवाने को भी तैयार रहते.
नौला, जहाँ से हम पानी भरकर लाते वहाँ नाशपाती का एक बड़ा-सा पेड़ था. उस पेड़ पर गाँव की जिस बुआ का अधिपत्य था वह हमेशा चौकस रहतीं कि उन नाशपतियों पर कोई हाथ न साफ़ कर दे. ऐसा करते देख लें जिसे, उसका नास करने वाली गाली देने को तत्पर … उस पेड़ की नाशपतियाँ ऐसी मीठी और रसीली कि हम अपना नाश करवाने को भी तैयार रहते. दोपहर में जब सब ओर गहन सन्नाटा हो जाता, नंदी बुआ झपकी ले रही होतीं तो हमारा झुण्ड पानी भरने के बहाने नौला पहुँच जाता. जब तक चाची, दीदी लोग अपनी गगरियाँ भरते, हम उचक-उचक कर बहुत सारे फल लपक लेते. सुए (तोता) और कव्वे के ‘ठूंक’ मारे नाशपाती ज्यादा मीठे निकलते….

दाड़िम तो बेशुमार… सबके घरों के आसपास और इधर-उधर भी. दाड़िम के बड़े-बड़े पेड़ों पर फूल आता तो वे लाल चुनरिया ओढ़े दुल्हन से दीखते. उनके झड़े फूल पंक्तिबद्ध बाराती बन हमारे खेल में शामिल रहते. हर पेड़ के दाड़िम का स्वाद अलग होता. पके दाड़िम पेड़ में ही फट कर दांत दिखा हँसते… फिर एक दिन सारे दाड़िम तोड़ कर आँगन में ढेर लगता. कुछ साबुत रख लिए जाते, बाकी को छीलकर गूदे निकालने का काम हम बच्चों को मिलता.बीच-बीच में आँख बचा हम मुठ्ठीभर मुँह में डाल ही लेते. बिछी हुई चादर में दाने निकाल सुखाने डाल दिए जाते और फिर साल भर उनसे खटाई पीसी जाती. अखरोट, दाड़िम और उसके गूदे बहुत समय तक संरक्षित किए जा सकते अत: आने-जाने वाले सम्बन्धियों को सौगात के रूप में भेंट किए जाते.
एक मीठे अनार का पेड़ था पौर के आँगन के किनारे … आँगन के भिड़ं में उसी की छाँव में लेट सुस्ताते थे बड़-बाज्यू. हम बच्चे उस पेड़ के अनार पर भी ललचाई नज़र रखते. हरेले के दिन उस पेड़ के अनार हमें देते बड़-बाज्यू… डिगारे की पूजा में अन्य मौसमी फलों के साथ वे अनार भी जगमगाते. दोपहर में अनार के नीचे सुस्ताते बड़-बाज्यू हम बच्चों से कहते… ‘मेरे सिर में कुरमुई लगाओ तो तुम्हें अनार मिलेगा’ तो हम झट से उनके ख्वाल्ट सर पर अपनी नन्हीं उँगलियाँ घुमाते ऊपर लगे अनारों पर टकटकी लगा रखते… उस के बाद ईनाम में मिलता अनार. विलायती आडू के पेड़ों से सुओं के झुंड को उड़ाने के लिए बड़-बाज्यू एक कनस्तर में रस्सी बाँध रखते और रस्सी हिलाने से बजते कनस्तर से फुर्र उड़ जाते सुओं के झुंड …
‘काफल’ तो पहाड़ की जान हुआ. रंग और रस से लबालब … काफल प्राय: जंगलों में पाया जाता. एक दिन गाँव की लडकियाँ, भाभियाँ, चाचियाँ मिलकर योजना बनातीं कि आज पार के धुर से काफल लाए जाएँ. सब झुण्ड बनाकर ठिठोलियाँ करती हुई पहुँच जातीं और पेड़ों में चढ़कर काफल इकठ्ठे किए जाते और टोकरियों में भरकर घर आते. उस दिन आँगन में काफल-उत्सव होता.
नींबू … भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार के… नारींग छोटा और बहुत मीठा, जामीर बला का खट्टा, और गलगल… नारियल के आकार का बड़ा-सा निम्बू सान कर खाया जाता. सर्दियों की गुनगुनी धूप में घर-भर की घरिनियाँ इकट्ठी हो निम्बुओं को छील-छाल देतीं और उसमें साना जाता दही, हरा धनिया-हरी मिर्च के साथ पिसा नमक, कतरी हुई मूली, गुड़ और भाँग, जी हाँ भाँग के पिसे दाने… हम सब घेरा बनाकर उसे सनते-बनते हुए देखते….फिर तीमिल के पत्तों में बंटकर चटकारे लेकर खाया जाता…

पहाड़ी ककड़ी भी… ‘काकड़’ कहलाती यह अनूठी नियामत पेड़ों या ठंगर में चढ़ी बेल में लटकी बहुत ही प्यारी लगती. पीले फूल के पीछे से अंगुल भर की निकलती ककड़ी को देखकर ही हमारा मन-मयूर नाच उठता… वह देखो ‘फुल्युड़’ … पर फुल्युड़ को तर्जनी दिखा दो तो माँ और आमा से बहुत डांट पड़ती. वह इतना संवेदनशील होता कि छुईमुई की तरह मुरझा जाता. हथेली भर का हो जाने पर हम काकड़ को चुराकर खाने की फिराक में रहते… कुछ और लम्बी हो जाए तो उसे चीरकर फाँके बना हरी मिर्च, लहसुन, अलसी के साथ पिसे नमक के साथ खाया जाता, जब पक कर पीला हो जाता, तब कोरकर राई वाला रायता बनता और अपने आखिरी दिनों में जब वह खूब गदराकर पीला हो उठता तब उसकी बड़ियाँ बनाई जातीं. काकड़ की झाल सूख जाने पर जब उसे हटाया जाता तब भी कुछ टेड़े-मेढ़े काकड़ उसमें मिल जाते.. उन्हें ढूँढकर खाने का भी अलग आनंद होता…
 पहाड़ी फलों की बात हो और ‘बेडू तथा काफल’ का रस न लिया जाए यह कैसे संभव है. इन दो फलों को तो मोहन उप्रेती जी ने अपने सुरों में पिरोकर विश्व-प्रसिद्ध कर दिया है. आप सबने सुना होगा न – “ बेडू पाको बार मासा, ओ नरेण काफल पाको चैता मेरी छैला…” ‘बेडू’ यानी अंजीर परिवार का मीठा गूदेदार रसीला फल. पककर बैंगनी रंग से ललचाता हुआ. बाहर का पतला-सा छिलका निकालो और गप्प से मुँह में जाते ही घुल जाने वाला. ‘काफल’ तो पहाड़ की जान हुआ. रंग और रस से लबालब … काफल प्राय: जंगलों में पाया जाता. एक दिन गाँव की लडकियाँ, भाभियाँ, चाचियाँ मिलकर योजना बनातीं कि आज पार के धुर से काफल लाए जाएँ. सब झुण्ड बनाकर ठिठोलियाँ करती हुई पहुँच जातीं और पेड़ों में चढ़कर काफल इकठ्ठे किए जाते और टोकरियों में भरकर घर आते. उस दिन आँगन में काफल-उत्सव होता. कोई नमक मिलकर तो कोई वैसे ही काफल की दावत उड़ाता.
पहाड़ी फलों की बात हो और ‘बेडू तथा काफल’ का रस न लिया जाए यह कैसे संभव है. इन दो फलों को तो मोहन उप्रेती जी ने अपने सुरों में पिरोकर विश्व-प्रसिद्ध कर दिया है. आप सबने सुना होगा न – “ बेडू पाको बार मासा, ओ नरेण काफल पाको चैता मेरी छैला…” ‘बेडू’ यानी अंजीर परिवार का मीठा गूदेदार रसीला फल. पककर बैंगनी रंग से ललचाता हुआ. बाहर का पतला-सा छिलका निकालो और गप्प से मुँह में जाते ही घुल जाने वाला. ‘काफल’ तो पहाड़ की जान हुआ. रंग और रस से लबालब … काफल प्राय: जंगलों में पाया जाता. एक दिन गाँव की लडकियाँ, भाभियाँ, चाचियाँ मिलकर योजना बनातीं कि आज पार के धुर से काफल लाए जाएँ. सब झुण्ड बनाकर ठिठोलियाँ करती हुई पहुँच जातीं और पेड़ों में चढ़कर काफल इकठ्ठे किए जाते और टोकरियों में भरकर घर आते. उस दिन आँगन में काफल-उत्सव होता. कोई नमक मिलकर तो कोई वैसे ही काफल की दावत उड़ाता.
और कैसे भूला जाए ‘हिसालु’ और ‘किल्मोड़ी’ को… ये तो पहाड़ी बच्चों के लंगोटिया यार हुए. पहाड़ में यत्र-तत्र-सर्वत्र पाए जाने वाले. कंटीली झाड़ियों में लदे हुए इन फलों को टीप टीप कर खाते हुए हम इस्कूल आते-जाते. हल्दिया रंग के नाजुक से हिसालु और किल्मोड़े के पीले खट-मिठ फूल से लेकर उसके पिद्दे-पिद्दे से हरे फल और पकने के बाद चमकीले स्लेटी, नीले, बैंगनी हो गए फल….
किमि, घिंघारू, तिमिल, स्यूंत, मेहव, पंय….
और भी जाने कितने बिसर गए स्वाद…
(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के इन्द्रप्रस्थ कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं)
