‘बाटुइ’ लगाता है पहाड़, भाग—10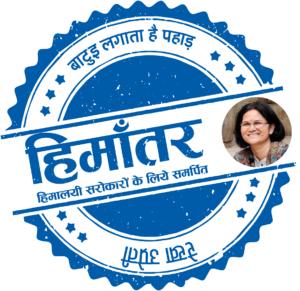
- रेखा उप्रेती
माघ की पहली भोर, पहाड़ों पर कड़कड़ाता जाड़े का कहर, सूरज भी रजाई छोड़ बाहर आने से कतरा रहा है, पर छोटे-छोटे बच्चे माँ की पहली पुकार पर उठ गए हैं. आज न जाड़े की परवाह है न अलसाने का लालच. झट से सबने अपनी ‘घुगुती माला’ गले में डाल ली है और छज्जे से बाहर झाँककर एक स्वर में गाने लगे हैं…
काले कावा काले
घुगुती मावा खाले…
पहाड़ छूटे चालीस बरस हो चुके हैं, पर मकर-संक्रांति पर मनाये जाने वाले ‘घुगुती-त्यार’ के दृश्य अब भी आँखों में तिरते हैं….
एक शाम पहले गुड़ के पाग में गूँथे आटे से विभिन्न आकृतियों के घुगुत बनाए जा रहे हैं. लोई को हथेलियों से पतले लम्बे रोल में बदल, उसे ट्विस्ट कर घुगुत का आकार दिया जा रहा है. बच्चे परात को घेर कर बैठे हैं. सबके हाथों में आटे की लोइयाँ हैं. कलाकारी दिखाने का अवसर है.
‘देखो, मैंने दाड़िम का फूल बनाया..’ एक कहता
‘और मैंने पान का पत्ता..’ दूसरी आवाज आती.
‘मेरी तलवार की धार तो देखो’ तीसरा स्वर गूँजता.
फिर ‘सिरून’ बनता, गोल-गोल सुपारी बनती, पूरी और खजूर बनते…आज माँ और दीदी का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है. जिसे जो बनाना है बनाए. माँ आखिर में सबकुछ तल देगी. अभी तो माँ उड़द दाल के बड़े बनाने में व्यस्त है, दीदी छोटी छोटी नारंगियाँ तोड़ रही है. रात को सब कुछ माला में पिरोया जाएगा और सुबह कव्वे को न्योंता मिलेगा…
माला में जितनी तरह की आकृतियाँ हैं, गीत में उतनी ही तुकबन्दियाँ . ‘लै कावा तलवार, मिकुं दिजा भलि-भलि सलवार… ( ले कौवा तलवार, मुझे देजा अच्छी-सी सलवार) माँगों की फ़ेरहिस्त लम्बी है. लै कावा बड़, मिकुं दिजा सुन घड़ (ले जा बड़ा, मुझको दे जा सोने का घड़ा..)
माला बनाते समय भी सब बच्चे चौकस हैं… कहीं मेरी माला में कोई कमी न रह जाए. गिनतियाँ सीखने का यह प्रत्यक्ष लाभ है कि हम अपने और दूसरे भाई-बहनों के घुगुते भी गिन सकते हैं. माँ सबके बराबर हिस्से कर रही है, सब अपनी अपनी माला सजा रहे हैं. बीचों-बीच रंगीन नारंगी, दोनों तरफ घुगुत और अपनी कलाकारी के नमूने… फिर अलग-अलग खूँटो पर मालाएँ टाँगकर रजाइयों में जा दुबके हैं, उत्साह के मारे नींद भी नदारद है…, कब सुबह होगी और हम कव्वौं को बुलाकर उनकी दावत करेंगे !! कोई हमसे पहले न कव्वौं को जिमा दे…

सुबह गाँव के हर आँगन में कटोरी भरकर सारे पकवान रखे जा रहे हैं और हर छज्जे पर मालाधारी नन्हे-मुन्ने विशिष्ट धुन में गा रहे हैं …
काले कावा काले…
घुगुती मावा खाले…
माला में जितनी तरह की आकृतियाँ हैं, गीत में उतनी ही तुकबन्दियाँ . ‘लै कावा तलवार, मिकुं दिजा भलि-भलि सलवार… ( ले कौवा तलवार, मुझे देजा अच्छी-सी सलवार) माँगों की फ़ेरहिस्त लम्बी है. लै कावा बड़, मिकुं दिजा सुन घड़ (ले जा बड़ा, मुझको दे जा सोने का घड़ा..)
हमारी माँगे तो बेमुरव्वत कव्वे ने कभी पूरी नहीं कीं, पर हम साल-दर-साल उसे पकवान खिलाने में कोई कमी नहीं बरतते. कव्वे आसमान में मंडराते, हम और जोर लगाकर गाते. जब तक हमारे आँगन की कटोरी पर कव्वा न झपटता तब-तक उसे टेरा जाता.
कव्वे को इतना महत्त्व देने के पीछे क्या परंपरा रही ठीक से नहीं मालूम. कोई लोक कथा कहती है कि किसी जन-प्रिय राजा की मौत कव्वे के रूप में आने वाली थी तो सारी प्रजा ने राजा की जान बचाने के लिए यह आयोजन किया. कव्वा पकवानों से भरमाया रहा और मौत टल गयी. एक कथा यह भी कि किसी राजकुमार की जान बचाने के कारण कव्वे को पुरस्कार स्वरूप यह भोज मिला … पर हमें कथा से क्या!! कव्वे ने हमारे आँगन से घुगुत उठा लिए और अब हमारी बारी……
मीलों दूर के बाज़ार में सजी रंग-बिरंगी दुनिया … लाल-गुलाबी रिबन, काँच की चूड़ियाँ, नंगलाली, काजल, बिंदियाँ, गुब्बारे और भी जाने क्या-क्या … ये चींजें आकर्षित करती हैं, भली लगती हैं, बस यही इनका मोल है. हम देख-देख कर मगन हैं… ख़रीद-फ़रोख्त की कोई दुविधा नहीं क्योंकि हमारे पास हामिद जितने पैसे भी नहीं हैं… ‘बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ’ वाला फक्कड़पन शायद वहीं से मिला है.
नहीं नहीं… अपनी माला से अभी नहीं तोड़ कर खाएँगे… पहले घर में बचे हुए या अड़ोस-पड़ोस से आए हुए पर हाथ साफ़ करेंगें. माँ ने परदेस में रहने वाले काका-ताऊ के बच्चों के नाम से भी मालाएँ बनाई हैं, वे भी हमारे ही हिस्से पड़ेंगी. अपनी माला के घुगुत तो बस दिन में दस बार गिनेंगे हम…. और धीरे-धीरे, बचा-बचा कर खाएंगे, …
मकर-संक्रांति का एक और आकर्षण था, ‘उतरैंणि कौतिक’ यानी उत्तरायण का मेला… बड़े लोग तो जाएँगे ही, ज़िद मान ली गयी तो हम भी साथ हो लेंगे. मीलों दूर के बाज़ार में सजी रंग-बिरंगी दुनिया … लाल-गुलाबी रिबन, काँच की चूड़ियाँ, नंगलाली, काजल, बिंदियाँ, गुब्बारे और भी जाने क्या-क्या … ये चींजें आकर्षित करती हैं, भली लगती हैं, बस यही इनका मोल है. हम देख-देख कर मगन हैं… ख़रीद-फ़रोख्त की कोई दुविधा नहीं क्योंकि हमारे पास हामिद जितने पैसे भी नहीं हैं… ‘बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ’ वाला फक्कड़पन शायद वहीं से मिला है.

उतरैंणि से जुड़ा एक लोकगीत भी कुछ-कुछ याद आता है. मुखड़ा नहीं सिर्फ एक अन्तरा..,
एक नन्हीं बच्ची मेले में जा रहे अपने दादा से पूछ रही है-
“ओ बड़बाज्यू! तुम मिहुणी के के ल्या ला…?” (बड़े बाबा! मेरे लिए क्या क्या लाओगे..?)
और उत्तर में दादा चुहल करते हैं-
“ मी तुहुणी बानर पोथीर ल्युनअ
ऊ दगड़ी त्यु खड्यूणी ब्या करूलअ”
(मैं तेरे लिए बन्दर का बच्चा लाऊँगा और उसके साथ तुझ मरी का ब्याह करूँगा)
‘खड्यूणी’ शब्द का कोई पर्याय हिंदी में ढूँढना असंभव है. कुछ कुछ पंजाबी की ‘मरजानी’ से मिलता-जुलता ज़रूर है, लेकिन इस शब्द में छिपे लाड़ और अपनेपन की मिठास को वही जान सकता है जिसने बचपन में अपने आमा-बड़बाज्यू के मुख से यह संबोधन सुना हो. इस तरह की अभिव्यक्तियाँ अब लुप्त हो रही हैं. भाषाएँ-बोलियाँ बचेंगी तो संस्कृतियों की विविध छवियाँ साँस लेंगी न …
(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के इन्द्रप्रस्थ कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं)

